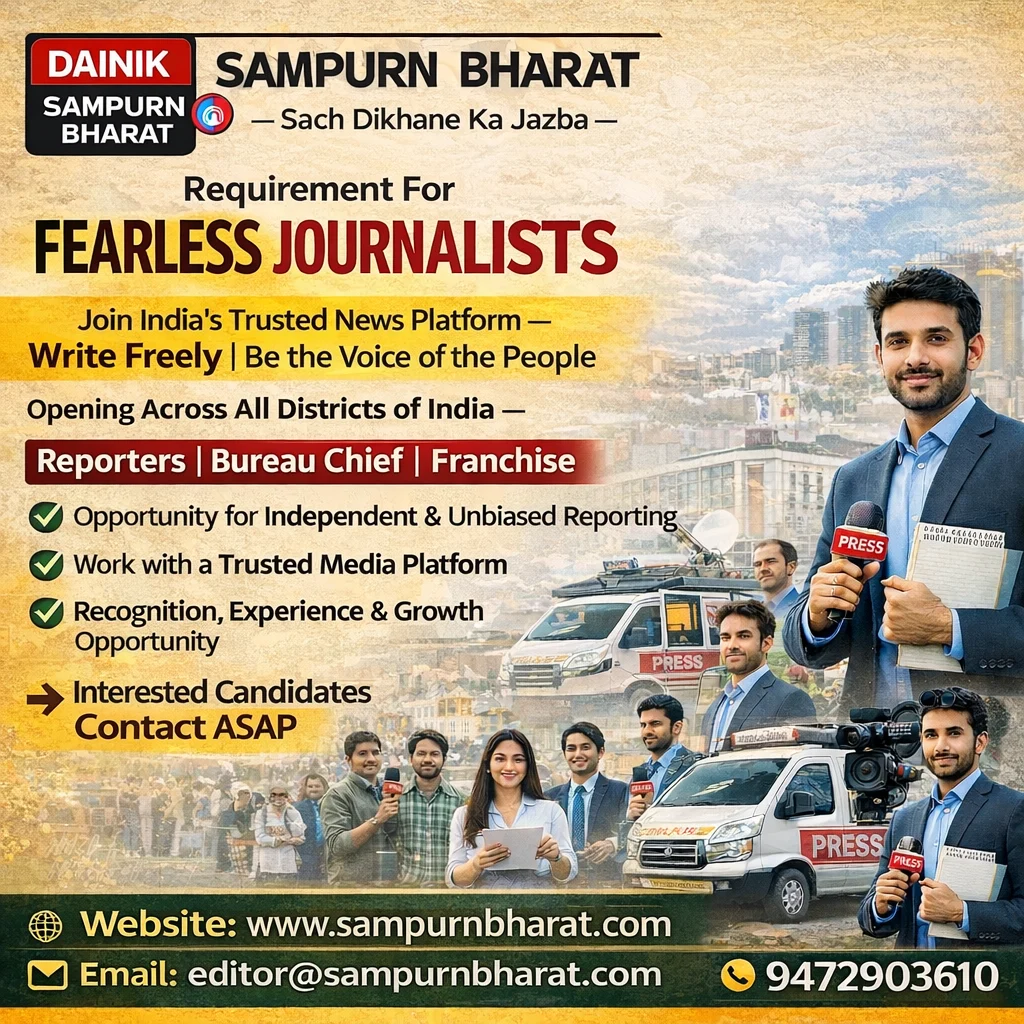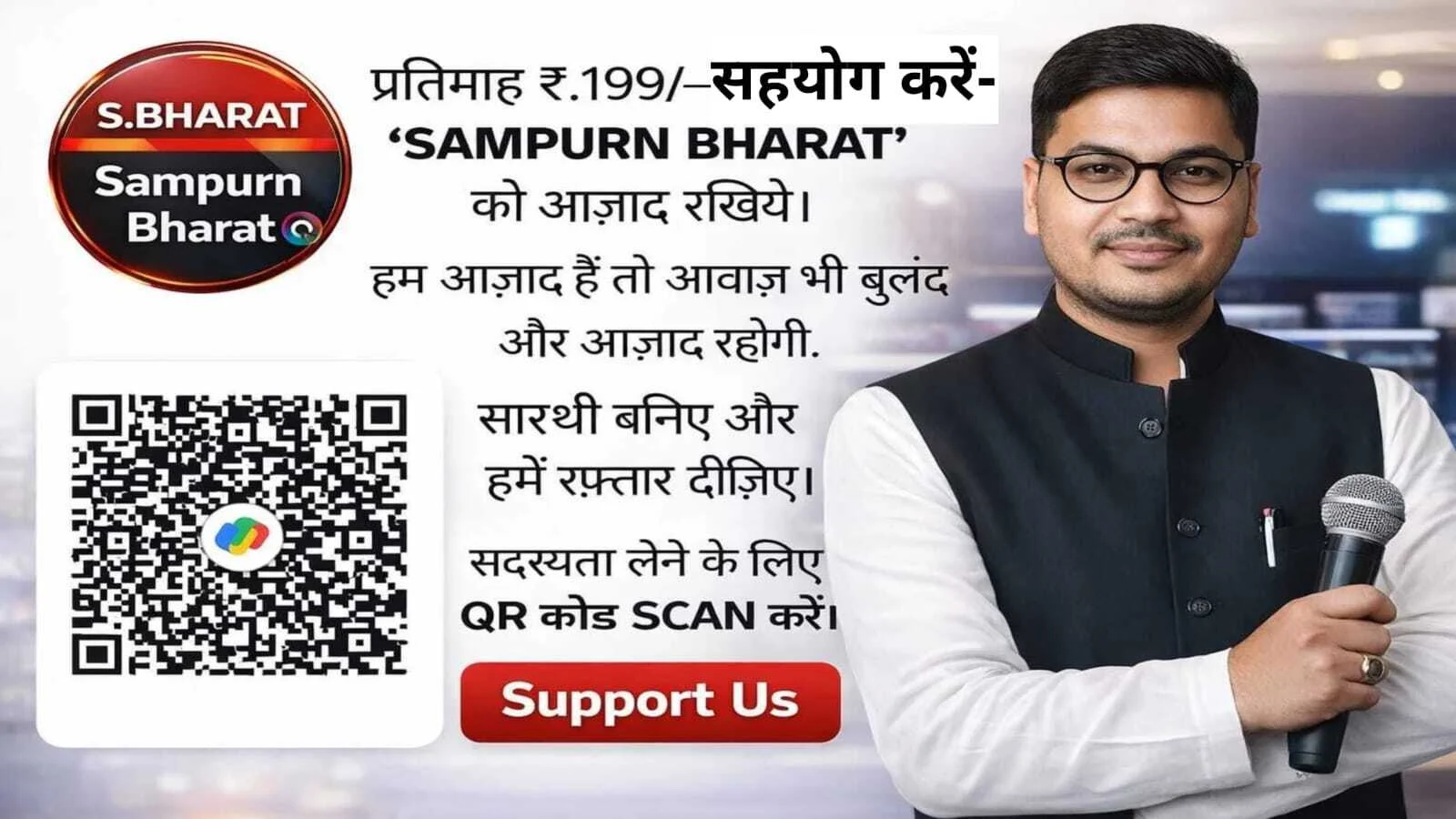काठमांडू/नई दिल्ली। नेपाल की राजनीति ने एक बार फिर तीखा मोड़ लिया है। सोशल-मीडिया प्रतिबंध से भड़के “Gen-Z” विरोध प्रदर्शनों ने पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को पद छोड़ने पर मजबूर किया और देश को एक अंतरिम चरण में धकेल दिया, जहाँ पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। यह बदलाव सिर्फ चेहरों का नहीं, नेपाल की विदेश-नीति की दिशा—खासतौर पर भारत और चीन के बीच संतुलन—का भी परीक्षण है।
क्या हुआ—घटनाक्रम संक्षेप में:-
- सरकार के सोशल-मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ विरोध व्यापक भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन में बदल गया; हिंसा और भिड़ंत के बीच कम से कम 51 मौतें दर्ज हुईं। इसके बाद प्रतिबंध वापस लिया गया और ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया।
- राष्ट्रपति ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया—नेपाल के इतिहास में पहली महिला पीएम।
भारत का रुख—सहयोग, संयम और नागरिकों की मदद:-
भारत ने आधिकारिक तौर पर संयम और संवाद की अपील की, हालात पर “करीबी नज़र” रखने की बात कही और नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए सलाह/हेल्पलाइन जारी की। यह संदेश साफ है—लोकतांत्रिक स्थिरता और शांति के पक्ष में खड़ा भारत, पड़ोसी के घरेलू टकराव को भड़काने नहीं, ठंडा करने की भूमिका निभाना चाहता है।
भारत की यह लाइन उचित है। संकट के क्षणों में सार्वजनिक बयानबाज़ी से अधिक मायने रखती है—कांसुलर सहायता, बैक-चैनल संवाद और चुनावी रोडमैप को quietly सपोर्ट करना।
विदेश-नीति पर कटाक्ष: “चाइना-कार्ड” और ओली की राजनीति:-
ओली के दौर में काठमांडू की भाषा कई बार “दिल्ली-संदेह” और “बीजिंग-नज़दीकी” जैसी दिखी—
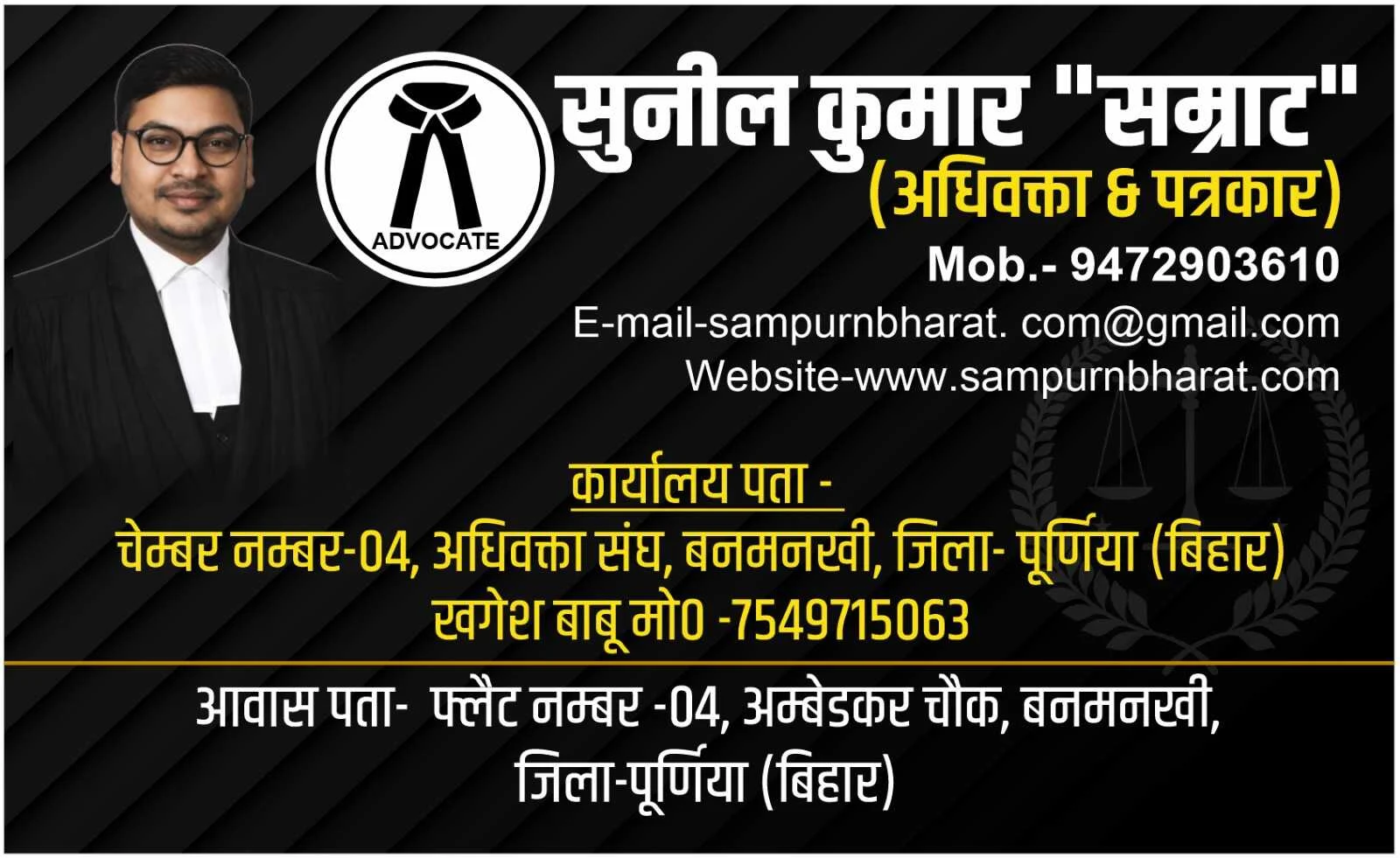
- 2020 में नए राजनीतिक नक़्शे के जरिए भारत-नेपाल सीमा विवाद (लिपुलेख/कालापानी/लिम्पियाधुरा) को उछाला गया—यह कदम घरेलू राष्ट्रवाद के लिए था, पर इससे भरोसे की खाई गहरी हुई।
- बीआरआई ढाँचे में नेपाल-चीन समझौते, पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा जैसे चीनी ऋण-निधि प्रोजेक्ट—राजनीतिक बयानों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक आर्थिक शर्तों और रणनीतिक निर्भरता का प्रश्न बनते दिखे; भारत के एयरस्पेस मुद्दे के कारण हवाईअड्डे की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अटकी रहीं—यानी निवेश, कूटनीति और भू-राजनीति एक-दूसरे में उलझ गईं।
- 2020 में काठमांडू के भीतर चीनी दूतावास/प्रतिनिधियों की सक्रिय मध्यस्थी की ख़बरें आईं—यह तस्वीर नेपाल की आंतरिक राजनीति में बाहरी footprints को दिखाती है।
- क्या चाइना-कार्ड खेलने से तात्कालिक राजनीतिक लाभ मिला? शायद। पर उसकी कीमत—सीमा-विवाद का तीखीकरण, ऋण-जोखिम और भारत जैसे जीवंत आर्थिक-सांस्कृतिक साझेदार से अनावश्यक खटास—अब उभरकर सामने है। नेपाल का व्यापार, ऊर्जा, रोज़गार-प्रवास और रोज़मर्रा की सप्लाई-चेन अभी भी बड़े पैमाने पर भारत पर टिकी है; इसलिए “रणनीतिक फुर्ती” का अर्थ संतुलन है, झुकाव नहीं।
कार्की का क्षण—संक्रमण की असली परीक्षा:-
सुशीला कार्की की पूँजी विश्वसनीयता है—न्यायपालिका से आईं, दलगत दबाव से अपेक्षाकृत दूर। पर संक्रमणकाल की चुनौती राजनीतिक है:
- शांति बहाली और जवाबदेही (प्रदर्शनों में मृतकों/घायलों पर विश्वसनीय जाँच),
- समयबद्ध चुनावी रोडमैप,
- डिजिटल अधिकार बनाम दुष्प्रचार पर संतुलित कानूनी ढाँचा।
संपादकीय रुख: कार्की सरकार का लिटमस टेस्ट यह होगा कि वह “Gen-Z” की ऊर्जा को संस्थागत सुधार में बदल पाती है या नहीं—सिर्फ कर्फ़्यू और प्रतिबंधों से स्थिरता नहीं आती।
नेपाल के लिए रास्ता—और भारत को क्या करना चाहिए
- तटस्थ संतुलन: नेपाल का दीर्घकालिक हित—भारत और चीन के बीच वास्तविक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। किसी एक धुरी पर टिके रहना, अगली राजनीतिक उथल-पुथल का बीज है।
- ऋण-अनुशासन: बीआरआई/अन्य ऋण-आधारित परियोजनाएँ वाणिज्यिक बनाम रणनीतिक कसौटियों पर कठोरता से परखी जाएँ; शर्तें पारदर्शी हों।
- भारत-नेपाल यथार्थवाद: ऊर्जा, कनेक्टिविटी, ट्रेड-फैसिलिटेशन में “क्विक-विन”—यही भरोसा बहाल करेगा। भारत को सार्वजनिक बयानबाज़ी कम, डिलीवरी-ड्रिवन सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए; यही उसकी silent strength है।
निष्कर्ष: सड़कों की आवाज़ और कूटनीति की समझ:-
नेपाल की नई कहानी युवा नागरिकता लिख रही है—जो भ्रष्टाचार-विरोध और डिजिटल-अधिकार को साथ लेकर चलना चाहती है। ओली-युग का “चाइना-कार्ड” दिखाता है कि भू-राजनीति में ओवर-करेक्शन हमेशा महँगा पड़ता है। भारत की भूमिका है—बिना शोर-शराबे के पड़ोसी की लोकतांत्रिक स्थिरता को ठोस सहयोग से सम्भालना। काठमांडू का भविष्य न तो सिर्फ नारे तय करेंगे, न केवल ऋण की पंक्तियाँ—उसे तय करेगी विश्वसनीय संस्थाएँ, पारदर्शी सौदे और एक ऐसी विदेश-नीति जो संतुलन को रणनीति का केंद्र बनाए।